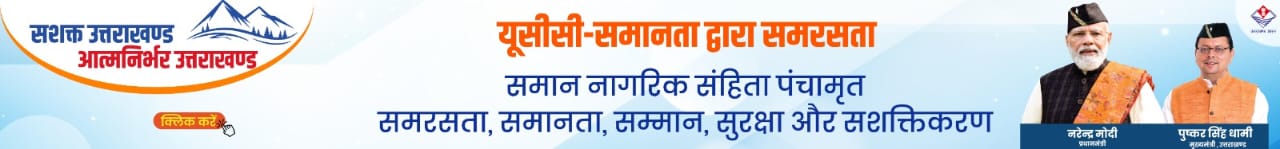डिजिटल निजता या लोकतंत्र पर नियंत्रण? – पत्रकारिता पर DPDP नियमों की चोट

डिजिटल निजता या लोकतंत्र पर नियंत्रण? – पत्रकारिता पर DPDP नियमों की चोट
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम (डीपीडीपी), 2025
पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर अदृश्य हमला
संपादकीय रवि सरन
भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 (DPDP Rules) को लागू करने का उद्देश्य था-नागरिकों की निजता को डिजिटल युग में सुरक्षित करना। लेकिन इन नियमों का वर्तमान स्वरूप लोकतंत्र के एक अन्य स्तंभ स्वतंत्र और निडर प्रेस के लिए एक गंभीर संकट बन गया है।
DPDP नियम जिस तरह से व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल को नियंत्रित करते हैं, वह केवल डिजिटल कंपनियों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, बल्कि पत्रकारोंपर भी वैसी ही कठोर शर्तें थोपता है। यह एक ऐसा कदम है जो लोकतंत्र में “जनता के जानने के अधिकार” को कानूनी जाल में फंसा सकता है।
पत्रकारिता पर नियामकीय शिकंजा
सच्चाई यह है कि खोजी पत्रकारिता अक्सर सत्ता से टकराती है, पर्दे के पीछे छुपी सच्चाइयों को सामने लाती है जिनमें व्यक्तिगत डेटा, गोपनीय दस्तावेज़ और संवेदनशील स्रोत शामिल होते हैं। लेकिन नए नियम कहते हैं कि डेटा के उपयोग से पहले “स्पष्ट सहमति” ली जाए, “उद्देश्य सीमाएँ” बताई जाएँ, और सभी सूचनाएँ “सटीक ” हों। इसका अर्थ है अब भ्रष्टाचार की कहानी लिखने से पहले भ्रष्ट व्यक्ति से अनुमति लेना होगी! यह न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि सच्चाई की हत्याजैसा है।
लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध
यूरोपीय संघ के GDPR जैसे कानूनों में पत्रकारिता को स्पष्ट छूट प्राप्त है। लेकिन DPDP नियमों में ऐसी कोई संवैधानिक या कानूनी सुरक्षा पत्रकारों के लिए नहीं है। धारा 8 में “उचित उद्देश्य” जैसी अस्पष्ट भाषा से उम्मीद की जा रही है कि पत्रकार खुद को कानूनी तौर पर सही साबित करें हर बार। इस पर निर्भर रहना पत्रकारों को एक उच्च-दांव वाले जुए में धकेल देता है: एक महत्वपूर्ण जाँच प्रकाशित करें और संभावित रूप से विनाशकारी जुर्माने (₹250 करोड तक) या लंबी, महंगी कानूनी लड़ाइयों का सामना करें, यह तर्क देते हुए कि उनका विशिष्ट कार्य इस अस्पष्ट मानक को पूरा करता है। यह न केवल एक भयकारी असमर्थताको जन्म देता है, बल्कि आत्म-सेंसरशिप और पैसे और मुकदमों के दबाव में संपादकीय स्वतंत्रता को खत्म कर देता है।
स्रोत की सुरक्षा पर आघात
पत्रकारिता का मूल स्रोत होता है व्हिसलब्लोअर, पीड़ित और इनसाइडर। लेकिन नियमों की सख्ती के चलते ऐसे स्रोतों से सहमति लेनाया सूचना देना उन्हें बेनकाब कर सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 17(2)(a) के अंतर्गत सरकार को इतने व्यापक अधिकार मिल जाते हैं कि वह किसी भी पत्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर डेटा माँग सकती है बिना पर्याप्त न्यायिक समीक्षा के। यह पत्रकारों को राज्य का उपकरणबनने पर मजबूर कर सकता है।
पत्रकारिता नहीं, जनहित संकट में
यह बहस केवल पत्रकारों की नहीं है। जब पत्रकारिता दबती है, तो जनता का जानने का अधिकार, भ्रष्टाचार की निगरानी और कमज़ोरों की आवाज़ सब कुछ दब जाता है। कोयला घोटाला हो या 2जी स्पेक्ट्रम, उजागर हुए ही इसलिए क्योंकि गोपनीय दस्तावेज़ सामने लाए गए। क्या DPDP नियमों के बाद वैसी खोजी रिपोर्टिंग संभव रह पाएगी?
आगे का रास्ताः संतुलन और संशोधन
निजता और पारदर्शिता दोनों हमारे संवैधानिक मूल्य हैं। लेकिन निजता की रक्षा करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बलि नहीं दी जा सकती। इस दिशा में तत्काल कदम आवश्यक हैं:
1. पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट जनहित में डेटा प्रोसेसिंग के लिए विधिक संरक्षण।
2. स्रोत की गोपनीयता की संवैधानिक गारंटी कोई संस्था पत्रकार से स्रोत नहीं पूछ सके।
3. उचित उद्देश्य की स्पष्ट परिभाषा ताकि पत्रकार कानून की अस्पष्टता में उलझें नहीं।
4. डेटा संरक्षण बोर्ड की स्वतंत्रता नियुक्ति और निगरानी में सरकार का हस्तक्षेप कम हो।
5. निगरानी सुधार और न्यायिक निगरानी अन्य कानूनों के साथ टकराव की स्पष्ट व्याख्या हो।
निष्कर्षः प्रेस की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र की ऑक्सीजन
DPDP नियम वर्तमान स्वरूप में “डिजिटल सुरक्षा की आड़ में लोकतंत्र को दमघोंटू” बना रहे हैं। यदि सरकार वास्तव में नागरिकों की स्वतंत्रता की पक्षधर है, तो उसे इन नियमों को पत्रकारिता के अनुकूल बनाने की ईमानदार पहल करनी होगी।
वरना, जैसा कि नेहरू ने कहा था-“मुझे एक स्वतंत्र प्रेस पसंद है, भले ही वह कभी-कभी ग़लत हो जाए, लेकिन एक दबा हुआ प्रेस लोकतंत्र का अंत है। “DPDP नियमों को अभिव्यक्ति की दीवार नहीं, बल्कि सूचना की पुल बनने देना होगा।